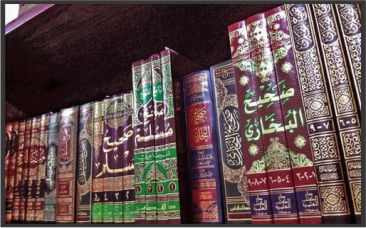Download eBook(pdf) : https://www.studyislam.in/hindi/Diyat_ki_Wastawikta.pdf
दियत की वास्तविकता
दियत क़ुरआन की एक शब्दावली है जो किसी की हत्या के अपराधी द्वारा अपनी जान बचाने के लिए मृतक के परिजनों को मुआवज़े के रूप में दी जाने वाली रक़म के लिए इस्तेमाल हुई है। यहां इस शब्द के अर्थ पर चर्चा की गयी है जिसके लिए लेखक ने शोध आधारित विवेचना की है। इस शब्द को आम उर्दू भाषा में ‘ख़ूनबहा’ कहा जाता है,
दियत (ख़ूनबहा) का जो क़ानून क़ुरआन में बयान हुआ है, उसके संदर्भ में आज के ज़माने में निम्न दो सवालों पर चर्चा होती रही हैः
एक यह कि दियत की कोई मात्रा क्या शरीअत में निर्धारित की गयी है और उसके अनुसार क्या मर्द के मुक़ाबले औरत की दियत वास्तव में आधी है ?
दूसरा यह सवाल कि दियत की वास्तविकता क्या है ? क्या यह उस आर्थिक नुक़सान का बदला है जो अपराधी की तरफ़ से मृतक के परिजनों को या घायल होने वाले को पहुंचता है, या जान या अंग की क़ीमत है, या इससे हट कर कोई तीसरी चीज़ है ?
पहले सवाल के जवाब में उन आयतों को देखते हैं जो इस क़ानून के संदर्भ में क़ुरआन में आई है।
क़ुरआन की चैथी सूरत “अलनिसा” में अल्लाह ने फ़रमाया है किः
“और किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि दूसरे मुसलमान का क़त्ल करे, मगर यह कि ग़लती से ऐसा हो जाए। और जो व्यक्ति इस तरह ग़लती से किसी मुसलमान को को क़त्ल कर दे तो उसके लिए यह ज़रूरी है कि एक मुसलमान को ग़ुलामी से आज़ाद करे और मृतक के वारिसों (परिजनों) को ख़ून बहा दे, यह अलग बात है कि वो उसे मआफ़ कर दें। फिर अगर मृतक तुम्हारी किसी दुशमन क़ौम का व्यक्ति हो लेकिन मुसलमान हो तो एक मुसलमान को ग़ुलामी से आज़ाद कर देना ही पर्याप्त है। और अगर वह किसी ऐसे समुदाय का व्यक्ति हो जिससे तुम्हारा शान्ति समझौता हो तो उसके वारिसों को भी ख़ूनबहा दिया जाएगा और तुम एक मुसलमान ग़ुलाम भी आज़ाद करोगे। फिर जिसके पास ग़ुलाम न हो, उसे लगातार दो महीने के रोज़े रखना होंगे। यह अल्लाह की तरफ़ से इस गुनाह पर तौबा (पाप के प्रायिश्चित) का तरीक़ा है और अल्लाह अलीम (सब कुछ जानने वाले) व हकीम (युक्ति पुर्वक काम करने वाले) हैं” 4: 92
इस आयत में “दियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही” के शब्द आए हैं। आम तौर से मानना यही है कि इन शब्दों को “ख़बर महज़ूफ़ का मुब्तदा” ( यानि एक ऐसी बात का शुरुआती जुमला जो शब्दों में न कही गयी हो लेकिन साफ़ समझ में आए) समझा जाए। यहां दियत शब्द “इस्मे नकरह” के रुप में इस्तेमाल हुआ है (यानि इसका अर्थ समान्य और व्यापक है, कोई विशेष नाम नहीं है)। “इस्मे नकरह” के बारे में हम जानते हैं कि यह अपने अर्थ निर्धारित करने के लिए डिक्शनरी, प्रचलन और भाषण के परिप्रेक्ष्य को समझने के अलावा किसी चीज़ का ज़रूरतमंद नहीं होता। जैसे क़ुरआन में अल्लाह ने फ़रमायाः “बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय काटो”। यहां गाय शब्द के लिए अरबी का शब्द “बक़रह” इस्तेमाल हुआ है जो इस आयत में “नकरह” है। इस वजह से यह बिल्कुल निश्चित बात है कि यहूदियों को वही जानवर काटने का हुक्म दिया गया था जिसके लिए अरब की डिक्शनरी में और अरबों की प्रचलित भाषा में “बक़रह” शब्द इस्तेमाल किया जाता था। वो अगर कोई सी भी गाय ज़िब्ह कर देते तो हुक्म निश्चित रूप से पूरा हो जाता। इसका मतलब यह हुआ कि अरबों की प्रचलित भाषा के हिसाब से बोलने वाला अगर उस चीज़ का ज़िक्र (जिसे ज़रूरी किया गया है), “इस्म नकरह” के रूप में करेगा तो उसका अर्थ यही होगा कि उसने हमें इस मामले में प्रचलन या रीति के अनुसरण का हुक्म दिया है। फिर ‘इस्म नकरह’ चूंकि एक आम शब्द होता है इस वजह से बयान के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई ख़ास बात न होगी तो इस का मतलब बिल्कुल आम समझा जाएगा और यह शब्द किसी ख़ास चीज़ पर लागू न होगा। चुनांचि इस आयत में दियत का अर्थ हैः ‘वह चीज़ जो दियत के नाम से जानी जाती है’, और परिजनों को दियत देने का मतलब निश्चित रूप से यह है कि दियत के नाम से जो चीज़ जानी पहचानी जाती है वह मृतक के परिजनों को दी जाए।
सूरत बक़रह (2) की आयत 178 में क़ुरआन में जहां “क़त्ले अमद” (जानबूझ कर हत्या) की दियत का हुक्म आया है वहां इस बात के साथ ‘मअरूफ़’ (जानी पहचानी बात) शब्द का इस्तेमाल हुआ है जिससे यह हुक्म और स्पष्ट हो जाता हैः
2:178
अनुवादः “फिर जिसके लिए उसके भाई की तरफ़ से कुछ रिआयत की गयी तो मअरूफ़ के मुताबिक़ उसकी पैरवी की जाए और जो कुछ भी ख़ूनबहा हो वह अच्छी तरह अदा कर दिया जाए”।
बक़रह और निसा सूरतों की इन आयतों से यह बात साफ़ है कि ग़लती से हत्या और जानबूझ कर हत्या, दोनों स्थितियों में क़ुरआन का हुक्म यही है कि दियत सामाजिक चलन और रीति के अनुसार दी जाए। पैग़म्बर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इसे अपने ज़माने में लागू किया। रिवायतों में इस सम्बंध में जो कुछ बयान हुआ है, वह उस समय अरब के प्रचलन को दर्शाता है, इसमें कोई चीज़ भी ख़ुद पैग़म्बर का अपना फ़रमान नहीं है।
अब सवाल यह है कि दियत के संदर्भ में अरब में क्या चीज़ प्रचलित थी? इस्लाम से पहले के युग के अरब शायरों और अरबों के जनजीवन का अध्यन करने से मालूम होता है कि शुरू में हर उस आदमी की दियत जिसका वंश क्रम किसी क़बीले से साफ़ तौर से जुड़ा हो, दस ऊंट निर्धारित थी। क़बीले के किसी सहयोगी और बान्दी के बेटे की दियत “सरीह” (किसी क़बीले का वंशज) की दियत की आधी और औरत की दियत मर्द की दियत के मुक़ाबले आधी थी। अग़ानी के लेखक ने “औस” व “ख़ज़रज” क़बीलों के बीच एक लड़ाई की घटनाओं को बयान करते हुए लिखा हैः
“और उनके यहां मौला यानी हलीफ़ (सहयोगी) की दियत पांच ऊंट और सरीह (क़बीले के अपने व्यक्ति) की दियत दस ऊंट निर्धारित थी”। (3/41)
“अलमुफ़स्सिल फ़ी तारीख़ुल अरब क़ब्ल अलइस्लाम “ के लेखक जव्वाद अली ने लिखा हैः
“और मृतक अगर बांदी का बेटा हो तो उसकी दियत सरीह की दियत के मुक़ाबले में आधी और औरत की दियत मर्द की दियत की आधी दी जाती थी”। (5/592)
कुछ क़बीले अपने मान सम्मान के आधार पर दोहरी (डबुल) दियत लेते और कुछ बख़्शिश व भेंट के रूप में दूसरों को दोहरी दियत देते थे। अलमुफ़स्सिल में ही है किः
“बयान किया जाता है कि ग़तारीफ़ यानि हारिस बिन अब्दुल्लाह बिन बक्र बिन यशकर की क़ौम के लोग अपने मृतक के लिए दो दियतें वसूलते थे और दूसरों को, अगर ख़ुद उन पर दियत देना लाज़िम हो जाए तो एक दियत देते थे। बनी आमिर बिन बक्र बिन यशकर के लिए जिनके पूर्वज आमिर ही को ग़ितरीफ़ कहा जाता था, दो दियतें और बाक़ी सारी क़ौम के लिए एक दियत निर्धारित थी। इसी तरह रिवायतों में आता है कि बनी असवद बिन रज़न इस्लाम पूर्व युग में दूसरों को दोहरी दियत अदा करते थे। (5/593)।
जव्वाद अली लिखते हैं किः
“और दोहरी दियत अदा करने की यह पाबन्दी किसी कमज़ोरी के चलते नहीं बल्कि उनकी तरफ़ से मृतक के परिजनों पर दया व कृपा के रूप में थी”। (5/593)
बादशाहों (सम्राटों) की दियत एक हज़ार ऊंट निर्धारित थी, और उसे “दियतुल मलूक” (बादशाहों की दियत) कहा जाता था। क़राद बिन हनश अलसारदी बनी फ़ज़ारह की प्रशंसा करते हुए कहता हैः
“और हमने कमान रहन रखी, फिर फ़ज़ारी के माल में से एक हज़ार ऊंट उसके लिए बदले के रूप में दिए गए।”
“यानि दस सौ ऊंट जो बादशाहों की दियत है, उसकी अदायगी के लिए सय्यार बिन अम्र ने कोशिश की और यह ज़िम्मेदारी बिना देर किए पूरी कर दी।”
पैग़म्बर सल्ल. की पैदाइश से कुछ वर्ष पहले इस रीति में एक असाधारण बदलाव आया। बयान किया जाता है कि पैग़म्बर साहब के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने नज़र मानी थी कि अगर अल्लाह तआला उन्हें दस बेटे देंगे तो वह उनमें से एक को क़ुर्बानी के लिए ज़िब्ह कर देंगे (बलि दे देंगे)। तो जब अल्लाह ने उनकी यह कामना पूरी कर दी तो उन्होंने भी अपनी नज़र पूरी करना चाही। किस बेटे को क़ुर्बान किया जाए इसके लिए लाट्री डाली गयी तो उसमें अब्दुल्लाह का नाम निकला। अब्दुल मुत्तलिब उन्हें क़ुर्बानी स्थल की तरफ़ ले जा रहे थे कि लोगों ने उन्हें रोका और बेटे के फ़िदये (बदले) में ऊंट ज़िब्ह करने का मशौरा दिया। उस ज़माने में, जैसा कि हमने बयान किया है, दियत की मात्रा दस ऊंट निर्धारित थी। चुनांचि दस दस ऊंटो और अब्दुल्लाह के नाम पर लाट्री डाली गयी। हर बार लाट्री अब्दुल्लाह के नाम पर ही निकली, यहां तक कि ऊंटों की गिनती सौ हो गयी। इस बार जब लाट्री डाली गयी तो सौ ऊंटों पर निकली। रिवायतों में आता है कि इस घटना के बाद अरबों, ख़ास तौर से क़ुरैश में दियत की मात्रा सौ ऊंट मान ली गयी। इब्ने अब्बास रज़ि. फ़रमाते हैः
“दियत उस ज़माने में दस ऊंट थी। यह अब्दुल मुत्तलिब हैं जिन्होंने सबसे पहले सौ ऊंट दियत तय की। इसलिए क़ुरैश और अरब में दियत की यही मात्रा प्रचलित हो गयी।
(अलतबक़ातुल कुबरा, इब्ने सअद, 1/58)
ज़ुहैर बिन अबी सलमा ने अपने कलाम में दियत की यही मात्रा बयान की है। अबस और फ़ज़ारा की लड़ाई में तीन हज़ार ऊंट दियत के रूप में अदा करने की वजह से अरब के दो सरदारों हरम बिन सिनान और हारिस बिन औफ़ की प्रशंसा करते हुए वह कहता हैः
“कई सौ ऊंटों के द्वारा घाव मिटाए जाएंगे। तो जो बिल्कुल निर्दाेष थे, थोड़े थोड़े करके ये ऊंट दियत के रूप में देने लगे।”
ज़ुहैर के इस शेअर से यह बात साफ़ है कि अबस और फ़ज़ारह के बीच लड़ाई में मारे गए लोगों की यह दियत क़िस्तों में अदा की गयी। अग़ानी में हैः
चुनांचि ये तीन हज़ार ऊंट थे जो तीन साल में अदा किए गए। (10/297)
इसी संदर्भ में ज़़ुहैर ने बयान किया है कि दियत के रुप में आम तौर से ’इफ़ाल” यानि छोटी उम्र के ऊंट दिये जाते थे। वह कहता है किः
“तुम्हारे पैतृक माल में से अलग अलग तरह के मवेशी जो इफ़ाल यानि अच्छी नस्ल के पूरे बूते हैं मृतकों के वारिसों की तरफ़ भेजे जाते हैं।”
‘इफ़ाल’ शब्द की ख़ासियत के बारे में “मुअल्लाक़ात “ के व्याख्याकार ज़ोज़नी लिखते हैः
“कवि ने ख़ास तौर से छोटी उम्र के ऊंटों का ज़िक्र इसलिए किया है कि दियत के रूप में दो साल के, तीन साल के, चार साल के ऊंट ही दिये जाते थे।” (शरह अलमुअल्लक़ात, अलज़ोज़नी, 80)
घाव लगाने यानि घायल करने की दियत भी अरब में प्रचलित थी। अरब की डिक्शनरियों का अध्ययन करने से पता चलता है कि प्राचीन अरब की भाषा में ‘अर्श’ और ‘नज़र’ के शब्द दूसरे अर्थों के अलावा इस अर्थ में भी इस्तेमाल किए जाते थे। “लिसानुल अरब” में है किः “अर्श का मूल अर्थ ख़दश (रगड़ या घाव) है। फिर यह उस माल के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा जो घावों की दियत के रूप में लिया जाता था। हिजाज़ को क्षेत्र में इसके लिए ‘नज़र’ शब्द इस्तेमाल होता था।” (लिसानुल अरब, 6/263)
अरब की इसी रीति को अल्लाह के रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने क़ुरआन के बयान के अनुसार, जैसा कि हम ने उपर लिखा है, अपने ज़माने में लागू किया। चुनांचि इस सिलसिले की कुछ रिवायतों में यह बात साफ़ तरीक़े से बयान हुई है कि अल्लाह के रसूल ने दियत के मामले उसी तरह बनाए रखे जिस तरह आपके नबी बनने से पहले अरब महाद्वीप में प्रचलित थे। दियत की मात्रा या संख्या में बदलाव के बारे में इब्ने अब्बास की जो रिवायत हम ने उपर नक़ल की है, उसमें वह फ़रमाते हैः
“क़ुरैश और अरब के दूसरे लोगों में दियत की मात्रा यही सौ ऊंट चल पड़ी और रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने भी पहले की तरह इसी को ठहराया।” (अलतबक़ातुल कुबरा, इब्ने सअद 1/89)
एक दूसरी हदीस में जिसे भाषाविद आम तौर से “मअक़ुलह” की मिसाल में पेश करते हैं और जो शब्दों के मामूली से बदलाव के साथ मुसनद अहमद बिन हंबल में भी नक़ल हुई है, यह बात इस तरह बयान की गयी हैः
“अल्लाह के रसूल सल्ल. ने क़ुरैश (मक्का वासियों) और अंसार (मदीना वासियों) के बीच समझौते के रूप में एक तहरीर लिखी, जिसमें यह बात भी थी कि हिजरत (मक्का से पलायन) करके आने वाले क़ुरैश अपनी पहली स्थिति पर बने रहेंगे और उनके बीच दियत के मामले उसी तरह होंगे जिस तरह पहले प्रचलित थे।” (लिसानुल अरब 11/462)
अलबत्ता यमन (दक्षिणी अरब) के क्षेत्र में रीति यही थी कि हत्या और घाव के विभिन्न रूपों में दियत की मात्रा शासक निर्धारित करेगा। अतः रसूल सल्ल. के ज़माने में यह क्षेत्र जब इस्लामी शासन के अन्तर्गत आया तो आप ने उसके सरदारों के नाम एक पत्र में दियत की वही मात्रा उनके लिए भी निर्धारित कर दी जो आपके अपने क्षेत्र में प्रचलित थीं। अलमुफ़स्सिल फ़ी तारीख़ अलअरब क़ब्ल अलइस्लाम में हैः
“दियत दक्षिण अरब के लोगों में भी इसी तरह प्रचलित थी, लेकिन उसके लिए कोई विधिवत क़ानून नहीं बनाया गया था, बल्कि उसकी मात्रा तय करने का मामला शासक के विवेक पर छोड़ दिया गया था।” (5/594)।
यमन वासियों के नाम रसूल सल्ल. का एक पत्र3 में निम्नलिखित बात कही गयी हैः
“जिसने किसी मुसलमान को अकारण मार डाला और उसका अपराध साबित हो गया तो उससे बदला लिया जाएगा, यह अलग बात है कि मृतक के परिजन दियत लेने पर राज़ी हो जाएं। इस स्थिति में जान (प्राण) की दियत 100 ऊंट होगी और नाक की भी जब वह पूरी काट दी जाए। जीभ और होंटों और फ़ोतों (अण्डकोशों) और पुरूष के लिंग की, पीठ और दोनों आंखों की दियत भी यही होगी। अलबत्ता एक पांव और एक हाथ में आधी दियत होगी। जो घाव दिमाग़ तक पहुंचे, उसमें एक तिहाई और जो पेट तक पहुंचे उसमें भी एक तिहाई होगी। इसी तरह जिस घाव से हड्डी सिरक जाए उसमें पन्द्रह ऊंट हैं। हाथ और पांव की हर उंगली में दस, दांत में पांच और जिस घाव में हड्डी खुल जाए उसमें भी पांच ऊंट होंगे।4
(3) घावों की दियत में जो अनुपात इस पत्र में बयान हुआ है, उस पर अगर ग़ौर किया जाए तो अद्ल व इंसाफ़ की दृष्टि से बिल्कुल मुकम्मल और अन्तिम बात है। राज्य के शासकों और विधान निर्माताओं को इस सम्बंध में क़ानून बनाते समय इसे सामने रखना चाहिए।
(4) यह शब्द सुनन नसई में ही इस पत्र की एक दूसरी रिवायत से लिए गए हैं, देखेः रक़म 4854
औरत के बदले में मर्द को क़त्ल किया जाएगा और जो लोग सोना ही दे सकते हैं, उनके लिए यह दियत एक हज़ार दीनार ठहरेगी (नसई, 4857)।
इस विवेचना से यह सच्चाई पूरी तरह खुल जाती है कि इस्लाम ने दियत की कोई निश्चित मात्रा हमेशा के लिए निर्धारित नहीं की है, न औरत और मर्द, ग़ुलाम और आज़ाद और काफ़िर व मोमिन की दियत में किसी फ़र्क़ को बनाए रखना हमारे लिए ज़रूरी किया है। दियत का क़ानून इस्लाम से पहले अरब में प्रचलित था। क़ुरआन ने जान बूझ की गयी हत्या या ग़लती से हत्या दोनों में उसी प्रचलन के मुताबिक़ दियत देने का हुक्म दिया है। क़ुरआन के इस हुक्म के अनुसार अब दियत हर ज़माने और हर समाज के लिए इस्लाम का एक लाज़मी क़ानून है, लेकिन इसकी मात्रा, इसके रूप और दूसरे सभी सम्बंधित मामलों में क़ुरआन का हुक्म यही है कि ‘मअरूफ’़ यानि सामाजिक चलन और रीति का अनुसरण किया जाए। नबी सल्ल. और चारों प्रथम ख़लीफ़ाओं ने दियत के फ़ैसले अपने ज़माने में अरब के चलन के मुताबिक़ किये। फ़िक़्ह और हदीस की किताबों में दियत की जो मात्राएं बयान हुई हैं, वह इसी चलन के हिसाब से हैं। अरब की यह रीति अरब वासियों की सभ्यता और सांस्कृतिक परम्पराओं पर आधारित थी। लगातार युग परिवर्तन के चलते इतिहास के पन्ने पलटते गए हैं और चैदह शाताब्दियां बीत गयी हैं। रहन सहन और तौर तरीक़ों में जम़ीन व आसमान का फ़र्क़ हो गया है। अब हम दियत में ऊंट दे सकते हैं, न ऊंटों के लिहाज़ से इस दौर में दियत का निर्धारण कोई अक़लमंदी की बात है। आक़िला (बुद्धिमता) की स्थिति बिल्कुल बदल गयी है और ग़लती से हत्या के ऐसे रूप अस्तित्व में आ गए हैं जिनकी कल्पना करना भी उस ज़माने में मुमकिन नहीं था। क़ुरआन की हिदायत (सीख) हर युग और हर समाज के लिए है, इसलिए उसने इस मामले में मअरूफ़ की पैरवी करने का हुक्म दिया है। क़ुरआन के इस हुक्म के अनुसार हर समाज अपनी ही रीति को अपनाने का पाबन्द है। हमारे समाज में दियत का कोई क़ानून चूंकि पहले से मौजूद नहीं है, इस वजह से हमारे विधान निर्माताओं को अधिकार है कि चाहें तो अरब की इस रीति को ही अपनाएं और चाहें तो इसका कोई विकल्प सुझाएं। वो जो रूप भी अपनाएंगे उसे अगर समाज स्वीकार कर लेता है तो हमारे यहां वह ‘मक़बूल’ हो जाएगा और वही “मअरूफ़” मान लिया जाएगा। फिर मअरूफ़ पर आधारित क़ानूनों के बारे में यह बात भी पूरी तरह स्पष्ट है कि स्थितियों और समय के बदलाव के साथ साथ उनमें बदलाव लाया जा सकता है और किसी समाज के “उलिल अम्र” (प्रधान लोग) अगर चाहें तो अपने सामूहिक हितों के हिहाज़ से उन्हें नए सिरे से तय कर सकते हैं।
हनफ़ी फ़िक़्ह के एक मुख्य आलिम इब्ने आबिदीन अपने आलेख नशरुल उर्फ़ में लिखते हैः
“जानना चाहिए कि फ़िक़ही निर्देश या तो ‘नस-ए-सरीह’ (क़रआन व सुन्नत के स्पष्ट निर्देश) से साबित होते हैं और यही पहला ढंग है, और या इज्तेहाद व राय (चिंतन और मत) से साबित होते हैं। इज्तेहाद व राय पर आधारित निर्देशों में से बहुत से वो हैं जिनका आधार इज्तेहाद करने वाले आलिम इस हैसियत से अपने ज़माने के प्रचलन पर रखते हैं कि वह अगर बाद में होने वाले किसी घटनाक्रम पर इज्तेहाद करते तो अपनी पहली राय के विपरीत राय देते। इसलिए वो इज्तेहाद की शर्तों में यह शर्त भी बयान करते हैं कि उसमें लोगों की आदतों का समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़माने में बदलाव के साथ बहुत से निर्देश भी बदल जाते हैं। इसकी बहुत सी वजहें हो सकती हैं जैसे चलन में बदलाव, आवश्यकता का दबाव, या लोगों की हालतों में इस वजह से किसी बिगाड़ की आशंका कि हुक्म अगर पहले जैसा बना रहा तो उनके लिए नुक़सान और कठिनाई का कारण होगा और हमारी उस शरीअत के नियमों के विपरीत होगा जो आसानी व सुविधा को पसन्द करती है और नुक़सान व बिगाड़ को दूर करने पर आधारित है।” (रसाइल इब्ने आबिदीन 125)।
रहा दूसरा सवाल, यानि यह कि दियत की वास्तविकता क्या है, तो इस मामले में दो ही दृष्टिकोण आम तौर से मान्य हैः एक यह कि यह जान की क़ीमत है, और दूसरा यह कि यह उस आर्थिक नुक़सान का बदला है जो अपराधी की तरफ़ से मृतक के परिजनों को या घायल होने वाले को पहुंचता है।
हमारे नज़दीक यह दोनों दृष्टिकोण विचारणीय हैं। जो लोग इसे जान की क़ीमत मानते हैं उनका यह मानना केवल मुग़ालते की वजह से है। प्राचीन (इस्लाम पूर्व युग के) अरब में हत्या के मामले क्रमशः सार (प्रतिशोध या इंतेक़ाम), क़िसास और दियत के रूप में तय किये जाते थे। सार, जैसा कि इस क्रम से स्पष्ट है, अरबवासियों के नज़दीक मूल उद्देश्य होता था। उनकी मान्यता थी कि मृतक की आत्मा पक्षी बन कर उड़ जाती है और जब तक उसका बदला न लिया जाए पहाड़ों और रेगिस्तानों में ‘अस्क़ूनी’ ‘अस्क़ूनी’ (‘मुझे पिलाओ’, ‘मुझे पिलाओ’) कह कर चीख़तरी रहती है। उनमें से कुछ लोग यह मान्यता रखते थे कि क़ब्र में वही मृतक ज़िन्दा रहता है जिसका बदला ले लिया जाए और अगर किसी का बदला न लिया जाए तो वह मर जाता है और उसकी क़ब्र में अन्धेरा छा जाता है। अपने इन अंधविश्वासों की वजह से वह ‘सार’ को प्राथमिकता देते थे और दियत तो एक तरफ़, ‘क़िसास’ के लिए भी किसी मजबूरी के चलते ही राज़ी होते थे। उम्मे शमला कहती हैः
“सो ऐ शमला! उठ और तैयार होजा और अपने दुशमनों से उस मुसीबत का बदला ले जो तुझे पहुंचाई गयी है, और देख क़िसास और दियत को किसी हाल में स्वीकार मत करना।”
अब्बास बिन मर्दास अलसलमी ख़ज़ाअह क़बीले के एक व्यक्ति आमिर को बदला लेने के लिए उक्साते हुए कहता हैः
“और वो तुम्हें जिस दियत का लालच देते हैं उस पर विचार भी मत करना इसलिए कि रिशतेदारी के बावजूद वो तुम्हारे पास ज़हर लेकर आए हैं”
इस्लाम में आ जाने के बाद भी इस मामले में उनकी भावनाएं किती उग्र थीं इसका अंदाज़ा मसूर बिन ज़ियादा के उन शेअरों से लगया जा सकता है जो उसने अपने पिता की हत्या के बाद मदीना का गवर्नर सईद बिन आस की तरफ़ से सात दियतों के प्रस्ताव के जवाब में कहे। वह कहता हैः
“क्या उस आदमी के बाद जो कोयकब पहाड़ के दामन में मिट्टी और पत्थर की क़ब्र में दफ़न किया गया है”
“मुझे नसीहत की जाती है कि मैं उस ज़ालिम पर दया करूं जिसने मुझे यह दुख दिया है। मेरी दया इसके अलावा और क्या हो सकती है कि मैं बदला लेने में कोई कमी न छोड़ूं।”
“मेरे चचेरो, अगर मैं आज या कल अपना बदला न ले सका तो क्या हुआ, ज़माने की उम्र बहुत लम्बी है।”
“अगर मैं बिन देर किए दुशमन पर चोट न लगाऊं या उसकी चोट का निशाना न बनूं तो मेरी क़ौम कभी किसी मुक़ाबले के लिए मुझे आवाज़ न दे।”
“तुम ने एक बार लड़ाई का सीना हम पर रख दिया है तो सुनो, हम ने भी फ़ैसला कर लिया है कि हम भी उसका सीना तुम पर रखे बग़ैर चेन न लेंगे।”
“मुझे वो लोग दियत का प्रस्ताव देते हैं और माल स्वीकार करने की प्रेरणा देते हैं जिनके बाप और भाई कभी किसी हत्यारे की तलवार का शिकार नहीं हुए।”
चुनांचि यह ऐसी ही भावनाओं का नतीजा था कि वो दियत को स्वीकार करने को अपमान की बात समझते थे और उसे मृतक का ख़ून बेचने के समान मानते थे। बनी नस्र बिन क़ईन के एक शायर रबी बिन उबैद का शेअर हैः
“ऐ ज़व्वाब मैं ने तेरा क़त्ल मआफ़ किया है न उक्काज़ के बाज़ार में सोदेबाज़ी के समय तेरा ख़ून बेचने (दियत लेने) के लिए खड़ा हुआ हूं।”
लेकिन यह बात साफ़ है कि इसका दियत की हक़ीक़त से कोई सम्बंध नहीं था। इसकी हैसियत केवल एक भावनात्मक अभिव्यक्ति की थी और क़त्ल व ख़ून के मामलों में इस तरह के भावनात्मक अर्थ बयान करने की मिसालें रात दिन हमारे सामने आती रहती हैं। इनके आधार पर दियत की वास्तविकता तय करना बात के समझने का कोई अच्छा उदाहर उदाहरण नहीं है। जिन लोगों ने इसे अपनाया है उनकी नज़र शायद इस तरफ़ नहीं गयी कि इंसान की जान और उसके शरीर के अंग हर क़ीमत से परे हैं। कोई मां, कोई बाप, कोई भाई, कोई बेटा इस कल्पना से कभी दियत स्वीकार करने पर तैयार नहीं हो सकता कि वह अपने मारे गए बेटे, भाई या बाप के ख़ून की क़ीमत वसूल कर रहा है। इसलिए अगर यह बात मानी जाएगी तो इसका नतीजा यही निकलेगा कि दियत का क़ानून जिस वजह से बना है वह वजह ही ख़त्म हो जाएगी।
रहे वो लोग जो इसे आर्थिक क्षति का बदल ठहराते हैं तो उन्होंने यह विचार बनाते समय शायद इस बात पर ग़ौर नहीं किया कि किसी चीज़ की वास्तविकता के लिए यह ज़रूरी है कि वह उसके सभी छोटे बड़े अंगों में पाई जाती हो। हर वह व्यक्ति जिसने दियत के क़ानून का अध्ययन सरसरी नज़र से भी किया है यह मानेगा कि दियत केवल जान जाने के बदले में ही नहीं बल्कि शरीर के समस्त अंगों जैसे नाक, कान, आंख, दांत की क्षति के लिए भी ठहराई गयी है। अब ज़ाहिर है कि इनमें कई अंगो की क्षति किसी आर्थिक नुक़सान का कारण नहीं बनती। दाढ़, दांत, हाथ की एक उंगली, पांव का अंगूठा जैसा कोई अंग अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो इससे आर्थिक रूप से आखि़र क्या नुक़सान पहुंचता है? दियत के पूरे क़ानून को सामने रख कर ग़ौर किया जाए तो यह बात स्पष्ट होती है कि दूसरे बहुत से कारणों से अलग, केवल इस विरोधाभास के आधार पर भी यह विचार सही नहीं समझा जा सकता।
दियत की वास्तविकता के बारे में अगर ये दोनों विचार सही नहीं हैं तो फिर दियत की वास्तविकता फिर है क्या? इस सवाल का जवाब समझने के लिए ज़रूरी है कि अरब की परम्पराओं को देखा जाए।
इस्लाम पूर्व अरब की शायरी में दियत का ज़िक्र कई जगह आया है। क़त्ल व रक्तपात की घटनाएं उनके जीवन में इतनी आम थीं कि ‘सार’, ‘क़िसास’ और ‘दियत’ के विषय उनके शायरों की शायरी के लिए जैसे हर समय सामने रहते थे। इसमें शक नहीं कि वो अपने इन शेअरों में आम तौर से दियत स्वीकार करने वालों को खीज दिलाते और उन्हें बदला लेने पर उक्साते थे लेकिन इस तरह की भावनात्मक स्थिति के परिवेश के बग़ैर वो अगर कभी दियत के विषय पर कुछ कहते हैं तो दियत की वास्तविकता भी आम तौर से उनके बयान से स्पष्ट हो जाती है।
ऐसे अवसरों पर वो दियत के लिए “ग़रामह” या उसका पर्यायवाची “मग़रिम”शब्द इस्तेमाल करते थे। अरबी भाषा में यह शब्द बिल्कलु उसी अर्थ में बोला जाता है जिस अर्थ में हम उर्दू में शब्द ‘तावान’ या ‘जुर्माना’ बोलते हैं। हमारी भाषा में जिस तरह हर उस माल के लिए जो किसी अपराध की सज़ा के रूप में अपराधी से वसूला जाए तावान शब्द या जुर्माना प्रचलित है, इस्लाम पूर्व अरब की भाषा में उसी तरह इसके लिए ‘ग़रामह’ शब्द इस्तेमाल होता था। दियत की वास्तविकता को उजागर करने के लिए प्राचीन अरब के शायरों ने, जैसा कि हमने कहा, यही शब्द प्रयोग किया है। ज़ुहैर बिन अबी सलमा कहता हैः
“वो ऊंट तावान के रूप में थोड़े थोड़े करके एक समुदाय दूसरे समुदाय को देने लगा, हालांकि देने वालों ने लेने वालों में चुल्लू भर ख़ून भी नहीं बहाया।”
दियत के बारे में यही धारणा बाद में भी चलती रही। उमवी युग के एक शायर अजीर अलसलूली का शेअर हैः
“तुम पीड़ित हो तो वह तुम्हारा बदला ले कर तुम्हें ख़ुश कर देता है, और तुम ज़ालिम हो तो तुम्हारा साथ देकर तुम्हें राज़ी कर देता है, और इस ज़ुल्म के नतीजे में तावान (यानि दियत) देते समय तुम जो बोझ भी उस पर डालते हो, वह अकेला उसके लिए काफ़ी हो जाता है।”
इससे स्पष्ट है कि दियत न तो आर्थिक नुक़सान का बदल है न मारे गए व्यक्ति के ख़ून की क़ीमत है, बल्कि वास्तव में यह केवल ग़रामह यानि तावान या जुर्माना है जो जानबूझ कर की गयी हत्या में क़िसास के विकल्प के रूप में और ग़लती से हुई हत्या में निश्चित रूप से दोषी पर लागू किया जाता है।
(1987)